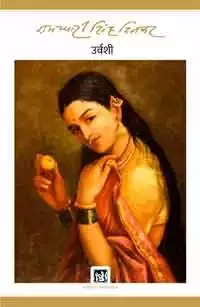|
लेख-निबंध >> साहित्य और समाज साहित्य और समाजरामधारी सिंह दिनकर
|
155 पाठक हैं |
||||||
प्रस्तुत पुस्तक में साहित्य की विभिन्न विधाओं और समस्याओं को समर्पित चिन्तापूर्ण अठारह निबन्धों का संकलन है।
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
साहित्य और समाज समर्थ साहित्यकार, ओजस्वी वक्ता और प्रखर चिन्तर
राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के साहित्य की विभिन्न विधाओं और समस्याओं
को समर्पित चिन्तन पूर्ण अठारह निबन्धों का संकलन है।
यह पुस्तक जहाँ एक तरफ- परम्परा और भारतीय साहित्य, साहित्य पर विज्ञान का प्रभाव, साहित्य में आधुनिकता, समाजवाद के अन्दर साहित्य, साहित्य का नूतन ध्येय, कलाकार की सफलता, भविष्य के लिए लिखने की बात; लेखकों का कार्य शिविर, हिन्दी साहित्य पर गांधीजी का प्रभाव, पाकिस्तान के पीछे साहित्य की प्रेरणा, श्री अरविन्द की साहित्यिक मान्यताएँ जॉर्ज रसल का साहित्य-चिन्तन आदि निबन्धों द्वारा समाज और साहित्य पर प्रकाश डालती है तो दूसरी तरफ़- अर्धनारीश्वर, कला, धर्म और विज्ञान, आउट-साइडर, रवीन्द्रनाथ की राष्ट्रीयता और अन्तर्राष्ट्रीयता अभारतीय हैं ?, महात्मा टॉलस्टॉय जैसे विषयों को भी हमारे सम्मुख लाती है।
पठनीय और मननीय निबन्धों से सुसज्जित यह पुस्तक राष्ट्रकवि दिनकर के चिन्तन स्वरूप को उद्घाटित करने वाली एक श्रेष्ठ बौद्धिक कृति है।
यह पुस्तक जहाँ एक तरफ- परम्परा और भारतीय साहित्य, साहित्य पर विज्ञान का प्रभाव, साहित्य में आधुनिकता, समाजवाद के अन्दर साहित्य, साहित्य का नूतन ध्येय, कलाकार की सफलता, भविष्य के लिए लिखने की बात; लेखकों का कार्य शिविर, हिन्दी साहित्य पर गांधीजी का प्रभाव, पाकिस्तान के पीछे साहित्य की प्रेरणा, श्री अरविन्द की साहित्यिक मान्यताएँ जॉर्ज रसल का साहित्य-चिन्तन आदि निबन्धों द्वारा समाज और साहित्य पर प्रकाश डालती है तो दूसरी तरफ़- अर्धनारीश्वर, कला, धर्म और विज्ञान, आउट-साइडर, रवीन्द्रनाथ की राष्ट्रीयता और अन्तर्राष्ट्रीयता अभारतीय हैं ?, महात्मा टॉलस्टॉय जैसे विषयों को भी हमारे सम्मुख लाती है।
पठनीय और मननीय निबन्धों से सुसज्जित यह पुस्तक राष्ट्रकवि दिनकर के चिन्तन स्वरूप को उद्घाटित करने वाली एक श्रेष्ठ बौद्धिक कृति है।
परम्परा और भारतीय साहित्य
यूरोप के एक लेखक ने लिखा है, ‘‘यूरोप नियम है, एशिया
मन की तरंग है। यूरोप कर्तव्य है, एशिया मनोदशा है। यूरोप तथ्यात्मक और वस्तुपरक है, एशिया वैयक्तिक और आत्मनिष्ठ है। यूरोप आदमी है, एशिया बच्चा और बूढ़ा आदमी है।’’
लेखक ने अपनी बात को जरा बढ़ा-चढ़ाकर कहा है, मगर सारत: उसकी उक्ति गलत नहीं है। मगर यह बात उस समय नहीं कही जा सकती थी, जब भारत संसार का ज्ञानगुरु और अग्रणी देश था तथा यूरोप बर्बरता की स्थिति से बहुत आगे नहीं बढ़ा था।
जातियाँ जिस प्रकार के विचारों में विश्वास करती हैं, उनके कर्म भी वैसे ही हो जाते हैं, उनकी कलाएँ भी वैसी ही हो जाती हैं। वैदिक युग के आर्य निवृत्तिवादी नहीं थे। दुनिया को वे केवल त्याग नहीं, भोग की भी वस्तु मानते थे। नरक की कल्पना उसके भीतर नहीं जगी थी। वे मानते थे कि पराक्रमी मनुष्य जैसे जीते जी सुख भोगता है, वैसे ही वह स्वर्ग पहुँचकर भी सुख ही भोगता है। ‘‘हे पितर, स्वर्ग में इन्द्र के साथ विहार कीजिए।’’ ‘‘हे इन्द्र, हमाके घोड़ों को मजबूत करो, हमारे पुत्रों को बलवान बनाओ।’’ ऐसी प्रार्थनाएँ वही कर सकता है, जो जीवन को सत्य तथा धरती को सुख और कर्म-कीर्ति का स्थान समझता है।
यद्यपि उपनिषद् वेदों के बाद ही प्रकट होने लगे थे, किन्तु संस्कृत साहित्य पर प्रभाव वैदिक विचारधारा का ही चलता रहा, उपनिषद् धीरे-धीरे ही काम करते रहे। जिसे साहित्य के कारण संस्कृत भाषा का संसार में इतना नाम है, वह सारा-का-सारा साहित्य वैदिक विचारधारा के अधीन लिखा गया था। उपनिषदों का प्रभाव संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ काव्यों पर नहीं के समान है। उपनिषदों की निवृत्तिमार्गी शिक्षा उस समय बढ़ी, जब देश में जैन और बौद्ध दर्शनों का जोर हुआ। वैदिक दर्शन आशावाद, सुख-भोग और उत्साह का दर्शन था। किन्तु हिन्दुओं का आज का दर्शन निवृत्ति, अहिंसा, वैराग्य और पस्ती का दर्शन है। यह मेरे विचार से उपनिषदों एवं बौद्ध और जैन दर्शनों के दीर्घ सेवन का परिणाम है और इसका प्रभाव हम संस्कृत के श्रेष्ठ काव्यों में कम, प्राकृत, अपभ्रंश और भारत की आधुनिक भाषाओं में अधिक देखते हैं। फिर भी यह सच है कि भारत का जो मन आज आधुनिक बनने का प्रयत्न कर रहा है, वह इसी निवृत्तिमार्गी संस्कार में रँगा हुआ है।
एक विचित्रता और है कि संस्कृत साहित्य में हमें विद्रोह का स्वर कहीं भी सुनाई नहीं देता है। गरीबी संस्कृत काल में भी रही होगी, अन्याय उस समय भी होते होंगे। जाति-प्रथा जितनी विषैली आज है, संस्कृत काल में उससे कहीं अधिक भयानक रही होगी। जो शूद्र वेद सुन ले, उसके कानों में पिघला हुआ रांगा पिला दो, यह धर्म उसी युग का आविष्कार था। किन्तु संस्कृत में कोई भी कवि ऐसा नहीं जनमा, जो यह कहने की हिम्मत करे कि यह अन्याय है और मैं इसका विरोध करूँगा। जन्मांतरवाद और कर्मफलवाद के सिद्धान्त इस जोर से स्वीकृति किए जा चुके थे कि हर चिन्तक यह सोचकर सन्तुष्ट था कि जहाँ भी जो कुछ हो रहा है, वह सब-का-सब ठीक है और विश्वविधान की आलोचना वही करेगा, जिसमें आस्तिकता की कोई गन्ध नहीं हो।
यहाँ यह भी ध्यान देने की बात है कि वैदिक युग के आर्य इतने अमर्षहीन नहीं थे, न उनकी स्वाधीन चिन्ता इतनी दबी हुई थी। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में ऋषि ने प्रश्न उठाया है कि जब कुछ नहीं था, तब क्या था और सृष्टि उसे शून्य में से कैसे प्रकट हुई और सृष्टि जब शून्य में से निकल रही थी, तब उसे किसने देखा था। और ऋषि ने स्वयं ही उत्तर दिया है कि इस सृष्टि का जो अध्यक्ष परम व्योम में रहता है, शायद उसने सृष्टि को जन्म लेते देखा हो अथवा क्या पता कि उसने भी नहीं देखा हो। एक आस्तिक ऋषि की यह शंका बतलाती है कि आर्य सत्य की शोध में बड़े ही निर्मोही और कठोर थे तथा श्रद्धा उनके चिन्तन को कमजोर नहीं कर सकती थी।
संस्कृत साहित्य में विद्रोही की परम्परा नहीं थी। भारत में विद्रोह के पहले बीज गौतम बुद्ध ने गिराए और वे अंकुरित चाहे जब भी हुए हों, पल्लवित और पुष्पित वे तब हुए, जब सुद्ध-साधुओं के समय आया। हिन्दी में इस विद्रोही की आग कबीर की वाणी में फूटी थी और वह आग अभी तक बुझी नहीं है। असल में भारतीय संस्कृति की दो धाराएँ हैं, जो प्रत्यक्ष देखी जा सकती है। एक के ऋषि मनुऔर वशिष्ठ, दार्शनिक शंकराचार्य और कवि तुलसीदास, सूरदार, विद्यापति, कम्बन और पोतन्ना हैं। दूसरी धारा के ऋषि स्वयं गौतम बुद्ध, दार्शनिक नागार्जुन और वसुबन्धु तथा कवि सिद्ध-साधु, कबीर, दादूदयाल, नानकदेव और वेमना हैं। आधुनिक युग में पहली धारा के प्रतीक महामना पंडित मदनमोहन मालवीय हुए हैं और दूसरी धारा के स्वयं गांधीजी। ज्यों-ज्यों समय बीतता जाता है, इन दो धाराओं के बीच की दूरी घटती जाती है। लेकिन दिखाई यह भी पड़ता बै कि धर्म के क्षेत्र में हिन्दू समाज तुलसीदास से हटकर कबीरदास के समीप होता जा रहा है। तुलसीदास का जितना जोर भक्ति पर था, उतना ही जोर व्रतों, अनुष्ठानों और धर्म के ब्राह्म आचारों पर ही था। किन्तु कबीरदास ने अनुष्ठानों को ढकोसला कहा। नए जमाने के धर्मानुरागियों की दृष्टि में भी अनुष्ठानों का कोई खास महत्त्व नहीं है।
साहित्य का स्वभाव है कि वह पुरानी बातों में कवित्व जरा अधिक देखता है। अतएव पुरानी परम्पराएँ आज भी साहित्य का विषय बन जाती है, किन्तु नवयुग का कवि उन्हें नई दृष्टि से देखता है और शिक्षा भी वह उनसे नई ही निकालता है। सत्यकाम-जाबाल की कथा पुराणों में यह दिखाने को गढ़ी गई होगी कि सत्य बोलने वाले को गोत्र के बारे में जिज्ञासा बेकार है। किन्तु अब हम उससे यह शिक्षा लेते हैं कि अनव्याही नारी की सन्तान भी सम्मान का आसन पा सकती है।
पहले धर्म और कविता के बीच प्रगाढ़ संबंध था। अब वह संबंध विरल भी नहीं रहा, बिलकुल टूट गया है। पहले के कवि कहते थे कि, ‘‘रसिक रीझेंगे तो समझूँगा कि मैंने कविता लिखी है। यदि रसिक नहीं रीझें, तो यह काव्य राधा और श्याम के नाम स्मरण का बहाना है।’’ आज धार्मिक कथा और चरित्र को भी कवि इसलिए नहीं उठाता कि उसे भगवान का स्मरण आता है, बल्कि इसलिए कि वह अपने सौन्दर्यबोध को अभिव्यक्त करना चाहता है। साहित्य में बहुत दिनों तक यह परिपाटी रही कि कविगण अपने काव्य का आरम्भ देवता की स्तुति से करते थे। लेकिन अब वह परिपाटी समाप्त हो गई। हिन्दी में राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त इस परिपाटी के अन्तिम उदाहरण थे। अब कोई भी कवि अपने ग्रन्थ का आरम्भ देव-स्तुति से नहीं करता।
एक विचित्रता घटित हुई है, जिसका उल्लेख प्रासंगिक लगता है। जब हम लोग काव्य के क्षेत्र में आए थे, कवियों में पिंगल पढ़ने का रिवाज था। एक कहावत चलती थी कि :
लेखक ने अपनी बात को जरा बढ़ा-चढ़ाकर कहा है, मगर सारत: उसकी उक्ति गलत नहीं है। मगर यह बात उस समय नहीं कही जा सकती थी, जब भारत संसार का ज्ञानगुरु और अग्रणी देश था तथा यूरोप बर्बरता की स्थिति से बहुत आगे नहीं बढ़ा था।
जातियाँ जिस प्रकार के विचारों में विश्वास करती हैं, उनके कर्म भी वैसे ही हो जाते हैं, उनकी कलाएँ भी वैसी ही हो जाती हैं। वैदिक युग के आर्य निवृत्तिवादी नहीं थे। दुनिया को वे केवल त्याग नहीं, भोग की भी वस्तु मानते थे। नरक की कल्पना उसके भीतर नहीं जगी थी। वे मानते थे कि पराक्रमी मनुष्य जैसे जीते जी सुख भोगता है, वैसे ही वह स्वर्ग पहुँचकर भी सुख ही भोगता है। ‘‘हे पितर, स्वर्ग में इन्द्र के साथ विहार कीजिए।’’ ‘‘हे इन्द्र, हमाके घोड़ों को मजबूत करो, हमारे पुत्रों को बलवान बनाओ।’’ ऐसी प्रार्थनाएँ वही कर सकता है, जो जीवन को सत्य तथा धरती को सुख और कर्म-कीर्ति का स्थान समझता है।
यद्यपि उपनिषद् वेदों के बाद ही प्रकट होने लगे थे, किन्तु संस्कृत साहित्य पर प्रभाव वैदिक विचारधारा का ही चलता रहा, उपनिषद् धीरे-धीरे ही काम करते रहे। जिसे साहित्य के कारण संस्कृत भाषा का संसार में इतना नाम है, वह सारा-का-सारा साहित्य वैदिक विचारधारा के अधीन लिखा गया था। उपनिषदों का प्रभाव संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ काव्यों पर नहीं के समान है। उपनिषदों की निवृत्तिमार्गी शिक्षा उस समय बढ़ी, जब देश में जैन और बौद्ध दर्शनों का जोर हुआ। वैदिक दर्शन आशावाद, सुख-भोग और उत्साह का दर्शन था। किन्तु हिन्दुओं का आज का दर्शन निवृत्ति, अहिंसा, वैराग्य और पस्ती का दर्शन है। यह मेरे विचार से उपनिषदों एवं बौद्ध और जैन दर्शनों के दीर्घ सेवन का परिणाम है और इसका प्रभाव हम संस्कृत के श्रेष्ठ काव्यों में कम, प्राकृत, अपभ्रंश और भारत की आधुनिक भाषाओं में अधिक देखते हैं। फिर भी यह सच है कि भारत का जो मन आज आधुनिक बनने का प्रयत्न कर रहा है, वह इसी निवृत्तिमार्गी संस्कार में रँगा हुआ है।
एक विचित्रता और है कि संस्कृत साहित्य में हमें विद्रोह का स्वर कहीं भी सुनाई नहीं देता है। गरीबी संस्कृत काल में भी रही होगी, अन्याय उस समय भी होते होंगे। जाति-प्रथा जितनी विषैली आज है, संस्कृत काल में उससे कहीं अधिक भयानक रही होगी। जो शूद्र वेद सुन ले, उसके कानों में पिघला हुआ रांगा पिला दो, यह धर्म उसी युग का आविष्कार था। किन्तु संस्कृत में कोई भी कवि ऐसा नहीं जनमा, जो यह कहने की हिम्मत करे कि यह अन्याय है और मैं इसका विरोध करूँगा। जन्मांतरवाद और कर्मफलवाद के सिद्धान्त इस जोर से स्वीकृति किए जा चुके थे कि हर चिन्तक यह सोचकर सन्तुष्ट था कि जहाँ भी जो कुछ हो रहा है, वह सब-का-सब ठीक है और विश्वविधान की आलोचना वही करेगा, जिसमें आस्तिकता की कोई गन्ध नहीं हो।
यहाँ यह भी ध्यान देने की बात है कि वैदिक युग के आर्य इतने अमर्षहीन नहीं थे, न उनकी स्वाधीन चिन्ता इतनी दबी हुई थी। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में ऋषि ने प्रश्न उठाया है कि जब कुछ नहीं था, तब क्या था और सृष्टि उसे शून्य में से कैसे प्रकट हुई और सृष्टि जब शून्य में से निकल रही थी, तब उसे किसने देखा था। और ऋषि ने स्वयं ही उत्तर दिया है कि इस सृष्टि का जो अध्यक्ष परम व्योम में रहता है, शायद उसने सृष्टि को जन्म लेते देखा हो अथवा क्या पता कि उसने भी नहीं देखा हो। एक आस्तिक ऋषि की यह शंका बतलाती है कि आर्य सत्य की शोध में बड़े ही निर्मोही और कठोर थे तथा श्रद्धा उनके चिन्तन को कमजोर नहीं कर सकती थी।
संस्कृत साहित्य में विद्रोही की परम्परा नहीं थी। भारत में विद्रोह के पहले बीज गौतम बुद्ध ने गिराए और वे अंकुरित चाहे जब भी हुए हों, पल्लवित और पुष्पित वे तब हुए, जब सुद्ध-साधुओं के समय आया। हिन्दी में इस विद्रोही की आग कबीर की वाणी में फूटी थी और वह आग अभी तक बुझी नहीं है। असल में भारतीय संस्कृति की दो धाराएँ हैं, जो प्रत्यक्ष देखी जा सकती है। एक के ऋषि मनुऔर वशिष्ठ, दार्शनिक शंकराचार्य और कवि तुलसीदास, सूरदार, विद्यापति, कम्बन और पोतन्ना हैं। दूसरी धारा के ऋषि स्वयं गौतम बुद्ध, दार्शनिक नागार्जुन और वसुबन्धु तथा कवि सिद्ध-साधु, कबीर, दादूदयाल, नानकदेव और वेमना हैं। आधुनिक युग में पहली धारा के प्रतीक महामना पंडित मदनमोहन मालवीय हुए हैं और दूसरी धारा के स्वयं गांधीजी। ज्यों-ज्यों समय बीतता जाता है, इन दो धाराओं के बीच की दूरी घटती जाती है। लेकिन दिखाई यह भी पड़ता बै कि धर्म के क्षेत्र में हिन्दू समाज तुलसीदास से हटकर कबीरदास के समीप होता जा रहा है। तुलसीदास का जितना जोर भक्ति पर था, उतना ही जोर व्रतों, अनुष्ठानों और धर्म के ब्राह्म आचारों पर ही था। किन्तु कबीरदास ने अनुष्ठानों को ढकोसला कहा। नए जमाने के धर्मानुरागियों की दृष्टि में भी अनुष्ठानों का कोई खास महत्त्व नहीं है।
साहित्य का स्वभाव है कि वह पुरानी बातों में कवित्व जरा अधिक देखता है। अतएव पुरानी परम्पराएँ आज भी साहित्य का विषय बन जाती है, किन्तु नवयुग का कवि उन्हें नई दृष्टि से देखता है और शिक्षा भी वह उनसे नई ही निकालता है। सत्यकाम-जाबाल की कथा पुराणों में यह दिखाने को गढ़ी गई होगी कि सत्य बोलने वाले को गोत्र के बारे में जिज्ञासा बेकार है। किन्तु अब हम उससे यह शिक्षा लेते हैं कि अनव्याही नारी की सन्तान भी सम्मान का आसन पा सकती है।
पहले धर्म और कविता के बीच प्रगाढ़ संबंध था। अब वह संबंध विरल भी नहीं रहा, बिलकुल टूट गया है। पहले के कवि कहते थे कि, ‘‘रसिक रीझेंगे तो समझूँगा कि मैंने कविता लिखी है। यदि रसिक नहीं रीझें, तो यह काव्य राधा और श्याम के नाम स्मरण का बहाना है।’’ आज धार्मिक कथा और चरित्र को भी कवि इसलिए नहीं उठाता कि उसे भगवान का स्मरण आता है, बल्कि इसलिए कि वह अपने सौन्दर्यबोध को अभिव्यक्त करना चाहता है। साहित्य में बहुत दिनों तक यह परिपाटी रही कि कविगण अपने काव्य का आरम्भ देवता की स्तुति से करते थे। लेकिन अब वह परिपाटी समाप्त हो गई। हिन्दी में राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त इस परिपाटी के अन्तिम उदाहरण थे। अब कोई भी कवि अपने ग्रन्थ का आरम्भ देव-स्तुति से नहीं करता।
एक विचित्रता घटित हुई है, जिसका उल्लेख प्रासंगिक लगता है। जब हम लोग काव्य के क्षेत्र में आए थे, कवियों में पिंगल पढ़ने का रिवाज था। एक कहावत चलती थी कि :
बिना कोक जो रति करे, बिन गीता भख ज्ञान,
बिना पिंगल कविता रचै, तीनों पशु समान।
बिना पिंगल कविता रचै, तीनों पशु समान।
लेकिन मेरा खयाल है, अब पिंगल कोई नहीं पढ़ता, न कोई प्रस्तार साधता है।
जब छन्द ही रुखसत हो गए, तब फिर पिंगल की जरूरत क्या है ?
पिंगल सीखते समय हमने यह भी शिक्षा ली थी कि ग्रन्थ ने आदि छन्द का प्रथम गण शुभ ही रखना चाहिए, अशुभ नहीं। तुलसीदासजी ने रामचरितमानस का आरम्भ ‘वर्णांना’ से किया है, जो मगण पड़ता है। हम लोग भी आदि गण, मगण, भगण नगण रखते थे। किन्तु, अब गणों का विचार भी खत्म है, न कोई कवि दग्धाक्षरों से डरता है।
पिंगल सीखते समय हमने यह भी शिक्षा ली थी कि ग्रन्थ ने आदि छन्द का प्रथम गण शुभ ही रखना चाहिए, अशुभ नहीं। तुलसीदासजी ने रामचरितमानस का आरम्भ ‘वर्णांना’ से किया है, जो मगण पड़ता है। हम लोग भी आदि गण, मगण, भगण नगण रखते थे। किन्तु, अब गणों का विचार भी खत्म है, न कोई कवि दग्धाक्षरों से डरता है।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book